मंचसज्जा और पात्रों के अलंकरण के लिए प्रयुक्त संसाधन और विधि विधान अति आवश्यक है। Manchsajjaa Aur Alankaran प्राचीनकाल में उलब्ध घरेलू सामग्री से ही किस प्रकार परिदृश्य-निर्माण और मेकअप की समस्याएँ ना किसी ताम-झाम और भारी व्यय को सरलता से उत्साही नाट्यप्रयोक्ताओं द्वारा प्रबंध कर लिया जाता है ।
इस परंपरा से आज भी लाभ उठाया जा सकता है-विशेष उन क्षेत्रों में जहाँ साधन और धन के अभाव में रंगमंच प्रगति नहीं कर सका। पात्रों की वेशभूषा, वर्ण, केश-विन्यास और आभूषणों का विवरण देते समय भरत ने तत्कालीन भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों, प्रदेशों और जातियों के रूपरंग, वेशभूषा और रीति-रिवाज के बारे में अपने विस्तृत ज्ञान का परिचय दिया है।
सर्वप्रथम भरत ने विभिन्न प्रदेशों के स्त्री-पुरुष द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों और मालाओं का वर्गीकरण किया है। आभूषणों को 4 भागों में विभाजित किया है :
1- आवेध्य : ऐसे आभूषण जो शरीर को वेध कर पहने जाएँ, जैसे कुंडल।
2- बंधनीय : जो बाँधकर पहने जाएँ, जैसे कर्धनी।
3- प्रक्षेप्य : जिन्हें किसी विशेष अंग पर सजाया जाए, जैसे नूपुर और अँगूठी।
4- आरोग्य : जिन्हें शरीर पर ऊपर से आरोपित किया जाए, जैसे हार।
मालाएँ पाँच प्रकार की बताई गई हैं :
1- वेष्टित : लपेटी हुई।
2- वितत : सीधी फैली हुई।
3- ग्रंथिम : बाँधी हुई।
4- प्रालंबित : लटकी हुई।
5- संघात्य : विशिष्ट प्रकार की माला जो उपर्युक्त मालाओं से भिन्न हो।
विभिन्न अंगों पर धारण किए जाने वाले आभूषणों की एक लंबी सूची दी गई है। आजकल इन आभूषणों का इतना प्रचलन नहीं है। इसलिए इनका विवरण देना उपयोगी नहीं होगा। लेकिन रंगकर्मियों द्वारा आभूषणों के प्रयोग के विषय में भरत ने कुछ उपयोगी सुझाव दिए हैं जिनका यहाँ उल्लेख करना आज के कलाकारों के लिए भी प्रासंगिक होगा।
आभूषण किसी विशेष कलाकार की रुचि के अनुसार नहीं बनने चाहिए और न एक कलाकार के द्वारा चाहे जितने अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। आभूषण शरीर के उपयुक्त स्थानों पर अलग-अलग पहने जाने पर ही शोभा बढ़ाते हैं। इनका निर्माण कलाकार के शरीर और आकृति को दृष्टि में रखकर ही करना चाहिए। प्रसंग के अनुसार अपनी बुद्धि से भी इनकी योजना की जा सकती है।
विभिन्न जातियों और प्रदेशों के स्त्री-पुरुषों के वेश और आभूषणों के बारे में नाट्यशास्त्र में विस्तृत जानकारी मिलती है। नागस्त्रियों के आभूषणों में मोती और रत्न जड़े हों और उनपर फण का चित्र अंकित हो। ऋषिकन्याओं के सिर पर बालों का जूड़ा हो और वस्त्र भी वनोचित हों। सिद्धस्त्रियों के आभूषण में मोती, मरकत और मणि का काम हो तथा उनके वस्त्रों का रंग पीला होना चाहिए।
गंधर्व स्त्रियों के आभूषणों में लाल मणि लगी हो; उनके वस्त्रों का रंग केसरिया हो और हाथ में वीणा हो। राक्षस स्त्रियों के आभूषण नीलम के बने हों, दाँत सफेद हों और वस्त्र गहरे नीले रंग का हो। दिव्य और वानर स्त्रियों के गहने पुखराज तथा लहसुनिया मणि से निर्मित हों तथा उनके वस्त्रों का रंग नीला हो। सुरनारियों के आभूषणों में मोती और लहसुनिया मणि लगे हों और उनके वस्त्र सुआपंखी रंग के हों।
दिव्य नारियों का यह वेश तब रखा जाए जब वे प्रेमासक्त हों, अन्यथा उनके वेश सादा और शुद्ध ही रखे जाएँ। अवंती देश की युवतियों के सिर पर लहरदार बाल होने चाहिए। गौड़ देश की स्त्रियों के बाल सामान्यतः धुंघराले हों। कभी-कभी उनका केश-विन्यास शिखापाश और वेणी की तर्ज पर भी हो सकता है।
अमीर स्त्रियों के बालों में दो वेणी होनी चाहिए और उनके सिर पर नीली चादर हो। पूर्वोत्तर प्रदेशों की स्त्रियों, की केश-शिखाएँ ऊपर उठी हों और उनका शरीर सिर तक वस्त्र से ढका रहे। दक्षिण देश की स्त्रियों के शरीर पर गुदना हो और उनका जूड़ा कुंभो-बंधक (मटका जैसा) शैली में बँधा हों। साथ ही उनके माथे पर बालों का गुच्छा लटका हो। गणिकाएँ अपनी रुचि के अनुसार अलंकार धारण कर सकती हैं।
जिन स्त्रियों का पति विदेश हो अथवा कष्ट में हो, उनके बाल साधारण एक चोटी में बँधे हों और शरीर अलंकार शून्य हो। विरहिणी नारियों का वेश शुभ्र, सामान्य और स्वच्छ हो तथा उनके शरीर पर एक-दो आभूषण ही होने चाहिए।
पुरुष पात्रों को सर्वप्रथम अपने शरीर के रंग का मेकअप करना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपनी भूमिका के अनुसार वेश बनाना चाहिए। शरीर के चार वर्ण बताए गए हैं-1. श्वेत, 2. श्याम, 3. पीत, 4. लाल। इसके अतिरिक्त कुछ रंगमिश्रित भी हो सकते हैं, जैसे पांडु (श्वेत-पीत), गुलाबी (श्वेत+लाल), सलेटी (नीला+पीला), कत्थई (नीला+लाल) और गोरा (लाल+पीला)।
पात्रों के शरीर को उपरोक्त वर्णों में दिखाने के लिए रंग तैयार करने की विधि भी बताई गई है। जहाँ तक एक ही रंग का प्रश्न है, उसके प्रयोग में कोई समस्या नहीं। कठिनाई वहाँ होती है जहाँ शरीर का मेकअप कई रंगों को मिलाकर करना पड़े।
मिश्रित रंग बनाने के लिए यह सावधानी बताई गई है कि जिस रंग को गहरा रखना हो, उसके दो भाग और जिस रंग को हलका रखना हो, उसका एक भाग लेना चाहिए। लेकिन जब नीला रंग मिलाना हो तब उसका एक भाग और दूसरे रंगों के तीन या चार भाग लेने चाहिए क्योंकि नीला रंग बहुत प्रबल होता है और इसकी थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है।
आजकल शायद मनचाहे तैयार रंग नाट्यकर्मियों को बाजार से मिल सकते हैं। लेकिन शौकीन नाट्यप्रयोक्ता भरत के उपरोक्त सुझावों का फायदा उठाते हुए सस्ते में ही घर पर मेकअप के रंग तैयार कर सकते हैं।
नाट्यशास्त्र में आगे देवी-देवताओं, मानवीय और अतिमानवीय पात्रों के शरीर का रंग बताया गया है और तदनुसार उनके शरीर का मेकअप होना चाहिए।
देवता, यक्ष और अप्सरा को गौर वर्ण में दिखाना चाहिए । रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य और स्कंद देवताओं का शरीर सुनहरी रंग का हो। चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, वरुण, नक्षत्र, गंगा, हिमालय और बलराम के शरीर का वर्ण शुभ्र रखा जाए। मंगल को लाल, बुध और अग्नि को पीला, नर-नारायण तथा नाग देवता वासुकी आदि को श्याम वर्ण का प्रस्तुत किया जाए। दैत्य, दानव, राक्षस और पिशाच का शरीर अश्वेत होना चाहिए। यदि जल, आकाश और पर्वत को मानवरूप में दिखाया जाए तो उनका रंग भी अश्वेत रखा जाए।
सप्तदवीप (भारत के पच्छिमोत्तर में स्थित देश) के निवासियों को गौर वर्ण में दिखाया जाए। जंबूद्वीप (भारतवर्ष) के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले पात्रों के अनेक रंग हो सकते हैं। कुरु प्रदेश को छोड़कर शेष उत्तरी भारत के निवासियों का रंग साफ और स्वर्ण के समान गोरा होना चाहिए।
भद्राश्व (संभवतः वर्तमान अफगानिस्तान) के लोगों का रंग श्वेत दिखाया जाए। भूतों का रंग कई प्रकार का हो और उनके चेहरे बकरी, भैंस, सुअर और हिरण जैसे पशुओं से मिलते-जुलते हों। राजाओं का रंग गुलाबी, श्याम या गोरा हो सकता है। सुखी और संपन्न व्यक्तियों का गौर वर्ण हो सकता है। दुराचारी व्याधिग्रस्त, तापसी और श्रमिक तथा निम्न वर्ग के पात्रों का रंग अश्वेत रखा जाए।
ऋषियों का रंग केसरिया हो लेकिन तपस्वियों को सदैव सलेटी रंग में दिखाया जाए। किसी विशेष कारण से अथवा पात्र की स्वयं अपनी इच्छा से शरीर का रंग देश, जाति और वय के अनुसार रखा जा सकता है। निदेशक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पात्रों का रंग देश, जाति, भूमिका और क्षेत्र के अनुरूप ही हो।
किरात, बर्बर आंध्र, द्रविड़, काशी, कौशल, पुलिंद (विंध्य प्रदेश की एक जाति) तथा दक्षिण के लोगों का रंग अश्वेत होना चाहिए। शक, यवन, पहलवी, बालीक और उत्तरी क्षेत्र के निवासियों को गौर वर्ण में दिखाना चाहिए। पांचाल, शौरसेन, माहिष, मगध, अंग, बंग तथा कलिंग देश के पात्रों का वर्ण श्याम होना चाहिए।
ब्राहमण और क्षत्रिय को गोरा तथा वैश्य एवं शूद्र को श्याम वर्ण दिखाना चाहिए। जिन क्षेत्रों और जातियों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे स्वभावतः भारत के प्राचीनकाल से संबंधित हैं। लेकिन उनका अस्तित्व आज भी परिवर्तित नामों से भारत में देखा जा सकता है। इसलिए पात्रों के रंग के विषय में भरत के उपरोक्त सुझाव आज भी उपादेय हो सकते हैं।
जहाँ तक दाढ़ी-मूंछों का प्रश्न है उनके चार प्रकार बताए गए हैं
1- श्वेत, 2- श्याम, 3- रोमश, 4- विचित्र। संन्यासी, मंत्री, पुरोहित और भिक्षु की दाढ़ी-मूंछ श्वेत होनी चाहिए। सिद्ध, विद्याधर, राजा, राजकुमार, युवराज, राजकर्मचारी, रसिक और यौवनमत्त पात्रों की दाढ़ी-मूंछ विचित्र होती है। वचन निभा न सकने के कारण लज्जित, दुःखी, तपस्वी और संकटग्रस्त पात्रों की दाढ़ी-मूंछ बढ़ी हुई रखी जाए। ऋषियों, संन्यासियों, व्रतधारी तथा वल्कलधारी मुनियों की दाढ़ी-मूंछ रोमश होनी चाहिए।
वेश तीन प्रकार का बताया गया है-1. शुद्ध, 2. मलिन, 3. विचित्र। मंदिर में जाते समय और कोई धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान करते समय पात्रों का वेश शुद्ध रहना चाहिए। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस, नृप और उच्च पदाधिकारी पात्रों का वेश विचित्र हो। वृद्ध ब्राह्मण, सेठ, मंत्री, पुरोहित, व्यापारी, कांचुकी, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य और पदाधिकारी पात्रों का केश भी शुद्ध होना चाहिए। पागल, नशेबाज, आपदग्रस्त और निम्न कोटि के पात्रों का वेश मलिन रखा जाए।
मुनि, जैन साधु, बौद्ध भिक्षु श्रोत्रिय और संन्यासी के वेश उनके व्रत और प्रथा के अनुसार होने चाहिए। तपस्वियों का वेश चीर-वल्कल और चर्म से तैयार किया जाए। परिव्राजक मुनि तथा बौद्धभिक्षुओं के वस्त्र भगवा रंग के होने चाहिए। पाशुपत संप्रदाय के लोगों का वेश विचित्र रखा जाए।
कुलीन स्त्री-पुरुषों का वेश उनकी हैसियत के अनुरूप होना चाहिए। राजा के अंतःपुर में नियुक्त व्यक्तियों का वेश भगवा रंग का और कवचयुक्त हो। योद्धाओं का वेश युद्ध के अनुसार और विचित्र अस्त्र-शस्त्र एवं कवच से युक्त होना चाहिए। वे तीर-कमान से भी लैस हों। राजाओं का वेश सदैव असामान्य रखा जाए। आपात्काल में अलबत्ता उनका वेश साधारण हो सकता है।
मुकुट तीन प्रकार के बताए हैं
1- पार्श्वगत, 2- मस्तकी, 3- किरीटी। पार्श्वगत मुकुट कनपटियों को ढक लेता था। मस्तकी मुकुट आगे माथे तक जाता था। किरीटी मुकुट चोटी पर ऊँचा रहता था और सिर का मुख्य भाग ढकता था। मुकुटों का यह वर्गीकरण आज भी प्रचलित है।
राजाओं का मुकुट मस्तकी होना चाहिए। विद्याधर, सिद्ध और गंधर्वो का मुकुट ऐसा हो जो उनके सिर के समस्त बालों को ढक दे। मंत्री, कंचुकी, सेठ और पुरोहित के सिर पर प्रतिशीर्ष (पगड़ी) रहनी चाहिए।
सेनापति और युवराज को अर्धमुकुट का प्रयोग करना चाहिए। शेष पात्रों के सिर पर परिधान उनकी जाति, देश, और हैसियत के अनुरूप और प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। साधुओं को जटाधारी होना चाहिए।
विचित्र पात्रों का केश-विन्यास भी बताया गया है। राक्षस, दानव और दैत्यों का रूप धारण करने वाले अभिनेताओं को भूरे बाल और हरी मँछ वाले चेहरे लगाने चाहिए । भूत-पिशाच, उन्मत्त तथा सामान्य साधु के बाल बिखरे होने चाहिए। बौद्धभिक्षु, जैनमुनि, श्रोत्रिय ब्राह्मण, संन्यासी और यज्ञदीक्षित पात्रों का सिर मुड़ा हआ रखा जाए।
राज्य के पदाधिकारी, गणिका और शौकीन व्यक्तियों के बाल धुंघराले हों। विदूषक का सिर गंजा या काकपक्ष (कनपटी) तक हो। साथ ही भरत ने पात्रों का केश-विन्यास देश और जाति के अनुसार रखने की छूट भी दे दी है। इस प्रकार आज के युग में बालों की जो फैशन हो, उसी को रंगकर्मी अपना सकते हैं। तलवार, ढाल, भाला, धनुष तथा लाठी आदि शस्त्रों के नाम और उनको बनाने की विधि भी नाट्यशास्त्र में दी हुई है।
इसके अतिरिक्त मुखौटा बनाने की विधि भी बताई गई है जो इस प्रकार है। सबसे पहले बेल के गूदा के गाढ़े घोल में कपड़े को भिगोकर एक पट्टी तैयार की जाए जिसकी लंबाई-चौड़ाई 32-32 अंगुल हो। इसे गीला ही रखा जाए। फिर बेल के पतले घोल में राख या धान का भूसा मिलाकर पेस्ट बनाया जाए और उससे चेहरे का सामने का हिस्सा बनाया जाए। जिस पर उपरोक्त गीली पट्टी चिपका दी जाए। पट्टी न बहुत पतली हो और न बहुत नर्म।
इस मुखौटे को धूप में रखकर सुखा लिया जाए फिर उसमें आँख, कान, नाक और मुँह बनाने के लिए छेद किए जाएँ। छेद करते समय चेहरे की लंबाई में दो बराबर भागों में बाँट लें। ऊपर के भाग में नीचे आँखें और नीचे के भाग के मध्य में मुँह दिखाया जाए। आँख और मुँह के बीच में तीन अँगल लंबे कानों के छेद किए जाएँ। मुँह का छेद भी इतना ही लंबा रखा जाए।
गर्दन 12 अंगुल ऊँची रखी जाए। आँखों के ऊपर भौंह रंग से बना दी जाएँ। आवश्यकतानुसार चेहरे के ऊपर रत्नजड़ित मुकुट भी कलात्मक ढंग से बनाया जा सकता है। रुचि और पात्र के रंग के अनुसार मुखौटा को रंग भी सकते हैं। इस प्रकार भरत के समय में नाट्यकर्मी मंचसज्जा और मेकअप की सभी सामग्रा स्वयं घरेल संसाधनों से तैयार कर लेते थे।
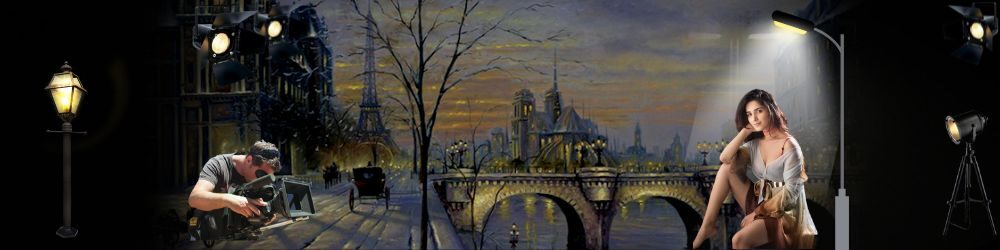


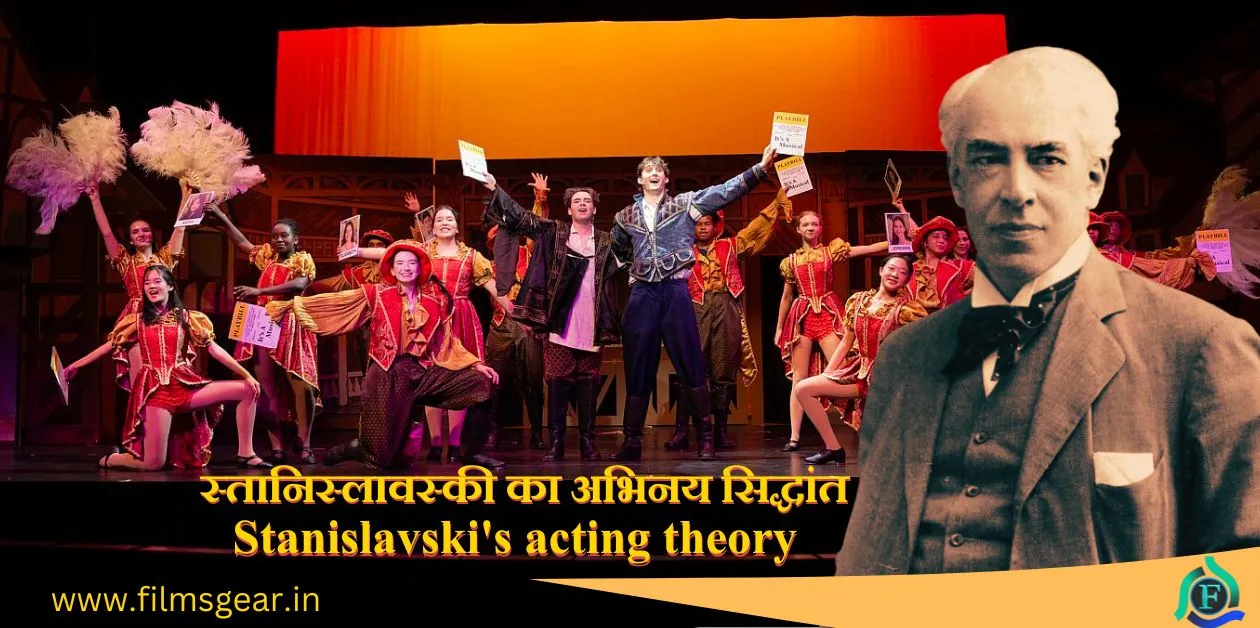

One thought on “Manchsajjaa Aur Alankaran मंचसज्जा और अलंकरण”